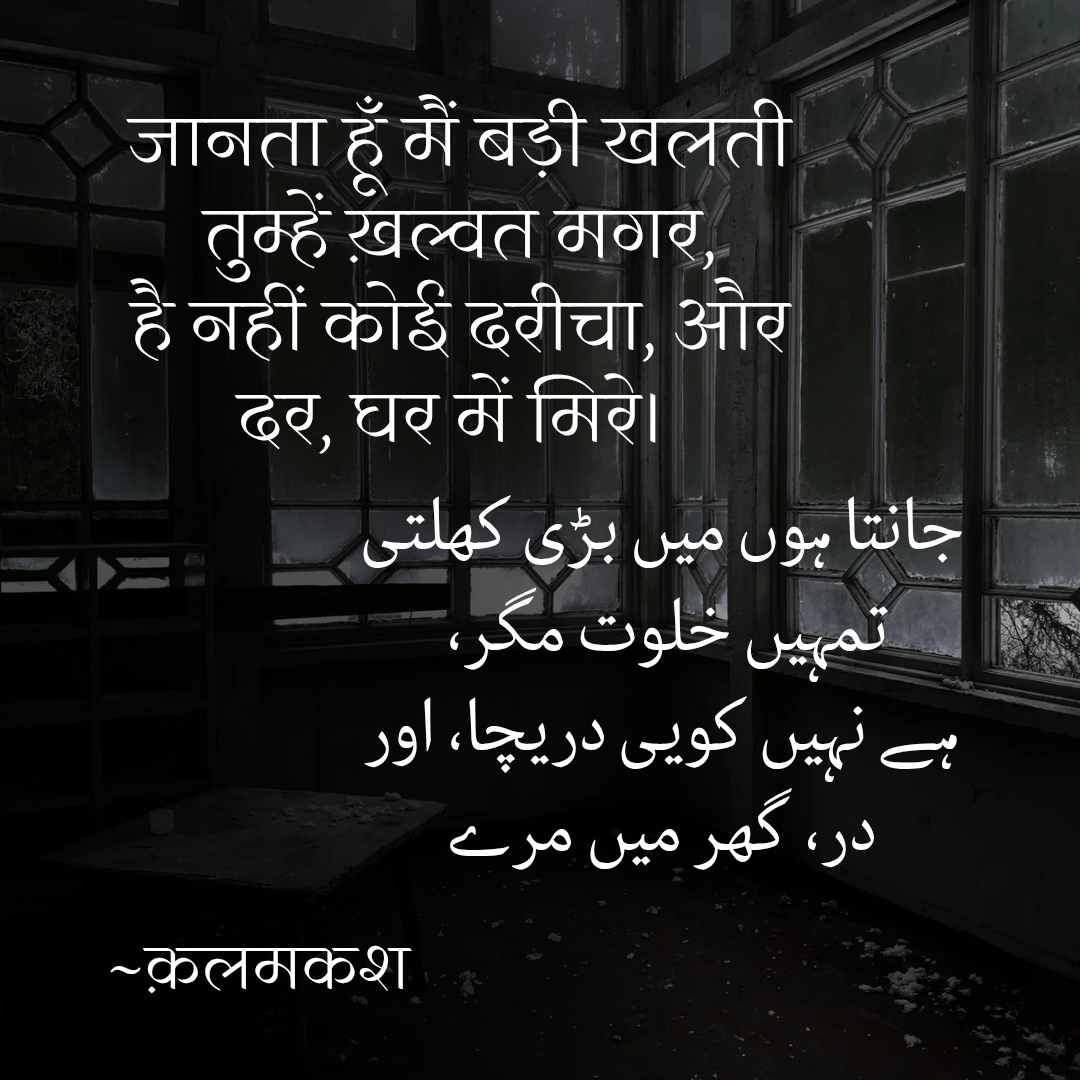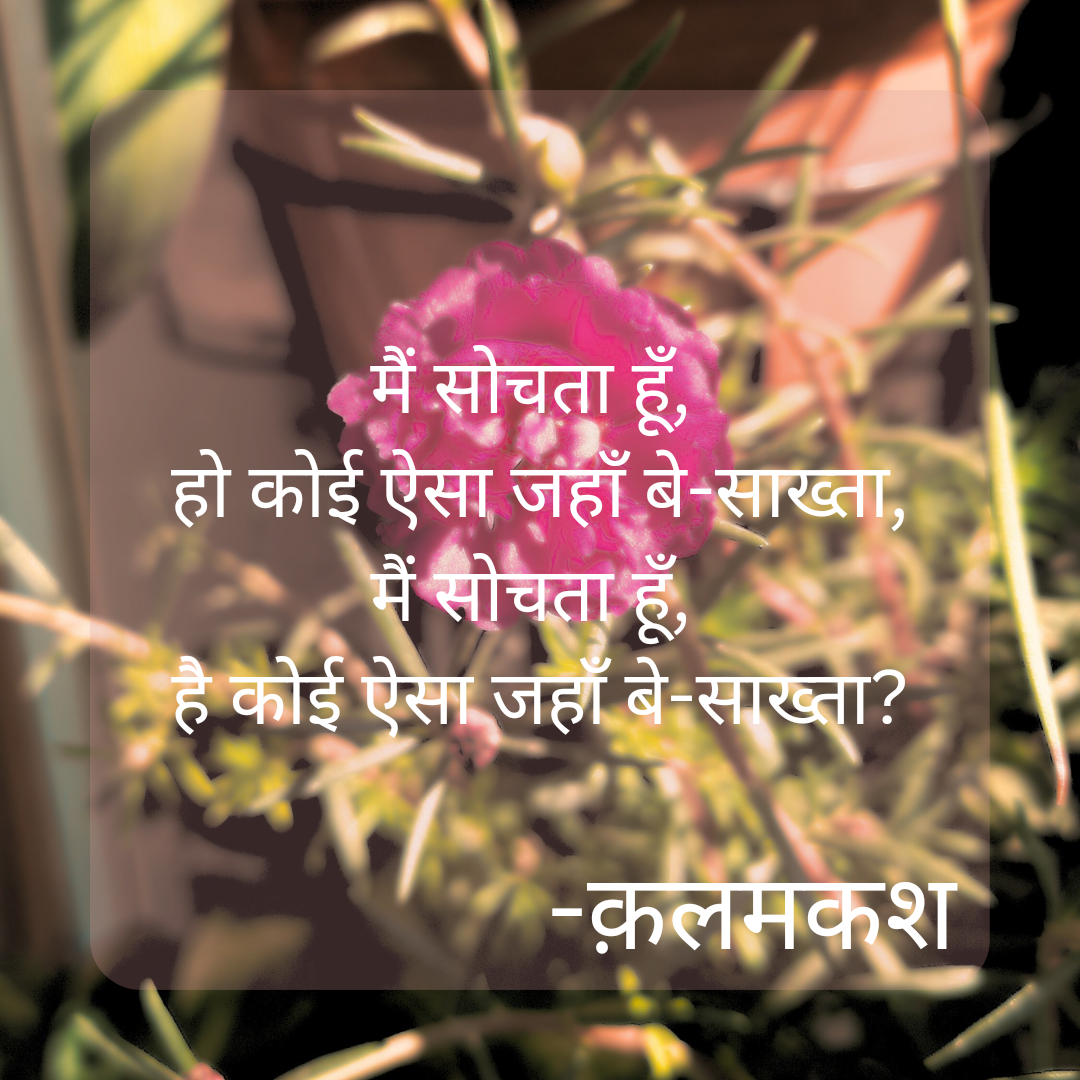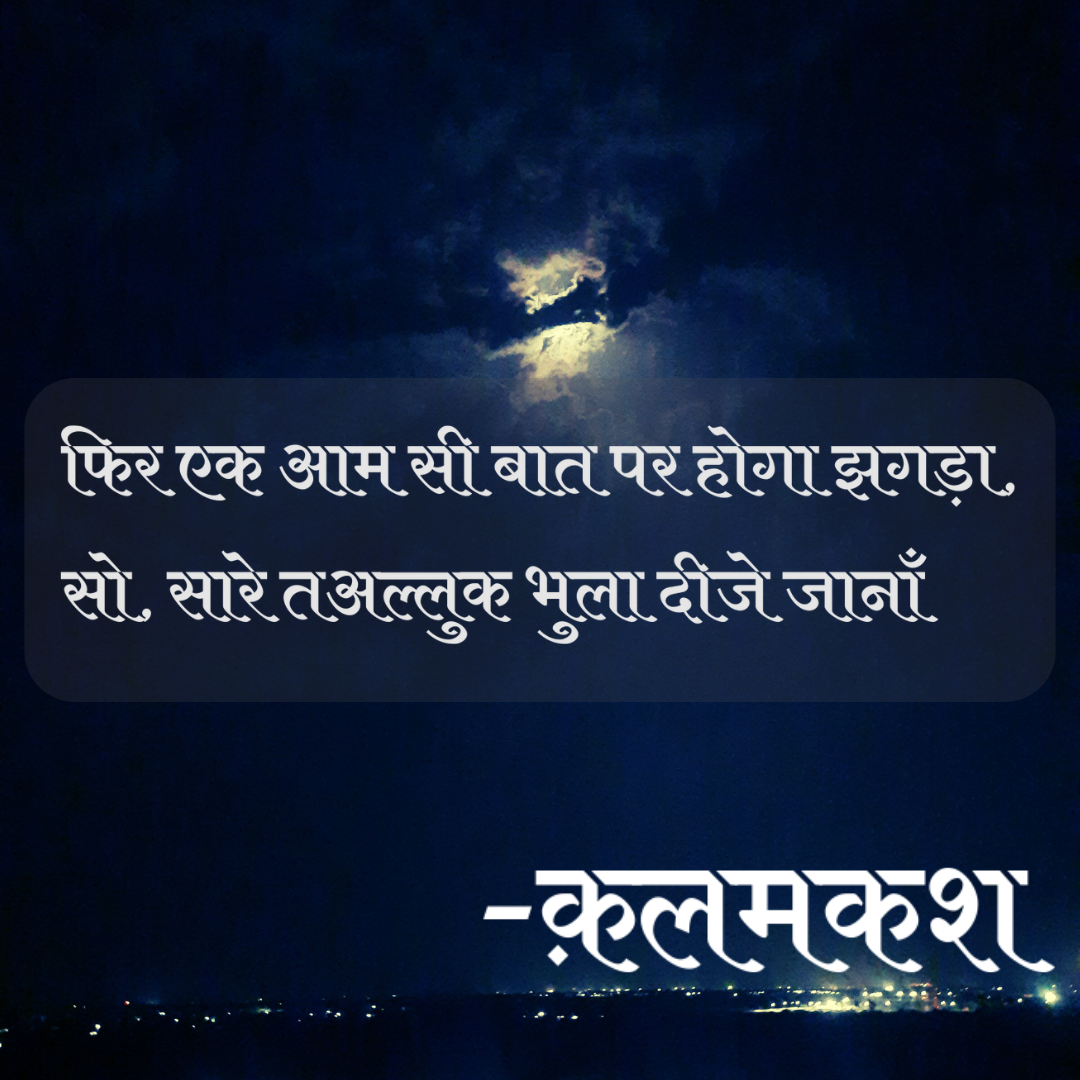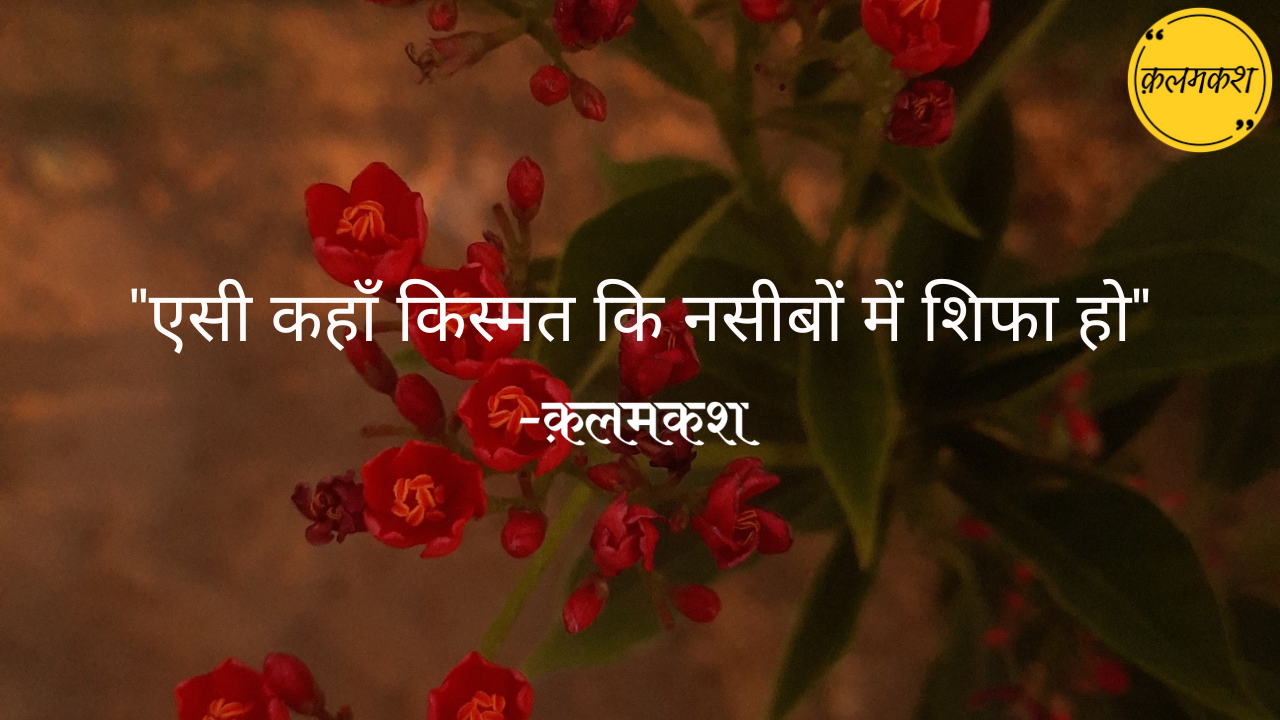ग़ज़ल: हैं नहीं आँसू तलक भी अब मुक़द्दर में मिरे
हैं नहीं आँसू तलक भी अब मुक़द्दर में मिरे,
ख़ूबियाँ कैसी हैं देखो तो सितमगर में मिरे।
था न-जाने कब से इक कतरा लहू का आँख में,
आज टपका तो दिखा क्या था तसव्वुर में मिरे।
तीर रहने दो जिगर में क्यों निकालें हम इसे,
इक यही तो याद दिलबर की रही घर में मिरे।
क्या करूँ ग़म जो मुझे अब बे-मुरव्वत कह दिया,
रोज़ क़िस्से लाख उड़ते हैं जहाँ भर में मिरे।
जानता हूँ मैं बड़ी खलती तुम्हें ख़ल्वत मगर,
है नहीं कोई दरीचा, और दर, घर में मिरे।